चंद्रगुप्त मौर्य: भारत के प्रथम सम्राट की विस्तृत जीवनी
🔰 भाग 1: प्रारंभिक जीवन एवं पृष्ठभूमि
1. जन्म एवं वंश
चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। उनके जन्मस्थान को लेकर विभिन्न मत हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि वे मगध क्षेत्र या उसके आस-पास के किसी ग्रामीण क्षेत्र में जन्मे थे। उनकी माता का नाम मोरा बताया जाता है, जिससे “मौर्य” नाम की व्युत्पत्ति मानी जाती है। कुछ ग्रंथों में उन्हें क्षत्रिय, तो कुछ में निम्न वर्ग से बताया गया है।
2. बाल्यकाल और सामाजिक परिवेश
चंद्रगुप्त का बाल्यकाल संघर्षपूर्ण था। उन्हें राजा धनानंद के दरबार से निष्कासित किया गया था। वे बाल्यकाल में गाय चराते थे और यहीं से उनके आत्मबल और नेतृत्व गुणों की झलक मिलती है।
3. चाणक्य से भेंट
तक्षशिला विश्वविद्यालय के ब्राह्मण आचार्य चाणक्य (विष्णुगुप्त/कौटिल्य) को जब नंद राजा ने अपमानित किया, तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे नंद वंश का नाश करेंगे। इसी क्रम में उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त से हुई। उन्होंने उसके भीतर राजा बनने की क्षमता देखी और तक्षशिला ले जाकर उसे शिक्षित किया।
4. शिक्षा एवं प्रशिक्षण
तक्षशिला में चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्धकला, कूटनीति, प्रशासन, गुप्तचर तंत्र और अर्थशास्त्र की शिक्षा दी गई।
5. प्रारंभिक असफलता
पहली बार जब चंद्रगुप्त और चाणक्य ने नंदों के विरुद्ध युद्ध किया, वे असफल हुए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पुनः संगठन करना शुरू किया।
6. सिंधु प्रदेश में सत्ता स्थापना
सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने यूनानी नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर कब्ज़ा जमाया और अपनी स्थिति मजबूत की।
7. अंतिम तैयारी
जनता के असंतोष का लाभ उठाकर उन्होंने पुनः नंदों के खिलाफ संगठित अभियान शुरू किया।
⛳ भाग 2: नंद वंश से संघर्ष और विजय
1. मगध की राजनीतिक स्थिति
चंद्रगुप्त के समय मगध पर नंद वंश का शासन था, जिसके अंतिम शासक थे धनानंद। वे अत्यंत धनी लेकिन क्रूर और अहंकारी माने जाते थे। उनके अत्याचारों और कर वृद्धि से जनता असंतुष्ट थी। यही असंतोष चंद्रगुप्त और चाणक्य के लिए अवसर बन गया।
2. चाणक्य की रणनीति
चाणक्य ने नंदों के विरुद्ध एक दीर्घकालिक योजना बनाई। उन्होंने गुप्तचर तंत्र, धन संग्रह, सैन्य संगठन और जनसमर्थन जैसे चार स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया।
3. युद्ध की शुरुआत
चंद्रगुप्त ने बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया। प्रारंभिक संघर्षों के बाद उन्होंने मजबूत सैन्य मोर्चा बनाया।
4. पाटलिपुत्र की घेराबंदी
अंततः चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र (राजधानी) को चारों ओर से घेर लिया। इस दौरान उनके सैनिकों को जनता का भी समर्थन मिला।
5. धनानंद की पराजय
तीव्र संघर्ष और चाणक्य की रणनीति के चलते नंद सेना पराजित हुई। धनानंद या तो युद्ध में मारा गया या निर्वासित कर दिया गया।
6. मौर्य साम्राज्य की स्थापना (322 ई.पू.)
चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठकर मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
7. विजय का महत्व
यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब एक शक्तिशाली और केंद्रीकृत साम्राज्य की नींव रखी गई।
⚔️ भाग 3: मौर्य साम्राज्य की स्थापना और शासन व्यवस्था
1. साम्राज्य का विस्तार
चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक फैला था। उन्होंने पहले पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी शासकों को हराया और फिर पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की।
2. यूनानी शासक सेल्यूकस से संधि
324 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद पश्चिमोत्तर भारत में सेल्यूकस निकेटर ने शासन किया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संघर्ष हुआ।
-
इस युद्ध में चंद्रगुप्त विजयी रहे।
-
एक संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और कंधार सौंपा।
-
बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी दिए।
-
इस संधि को और मजबूत करने के लिए चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह भी किया।
3. प्रशासनिक व्यवस्था
चंद्रगुप्त का शासन अत्यंत सुव्यवस्थित था। चाणक्य की सहायता से उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया।
(i) केंद्रीय प्रशासन
-
सम्राट के अधीन केंद्रीय मंत्री परिषद होती थी।
-
इसमें महापौर, सेनापति, महामात्य, कर अधिकारी, गुप्तचर प्रमुख आदि होते थे।
(ii) प्रांतीय व्यवस्था
-
साम्राज्य को कई प्रांतों में बाँटा गया। प्रत्येक प्रांत में ‘कुमार’ या ‘राजकुमार’ शासक होता था।
(iii) नगर व्यवस्था
-
पाटलिपुत्र जैसे नगरों में नगराध्यक्ष, व्यापार निरीक्षक, जलप्रबंधक आदि अधिकारी होते थे।
(iv) न्याय प्रणाली
-
न्यायपालिका सम्राट के अधीन थी। गंभीर अपराधों के लिए विशेष दंड निर्धारित थे।
4. कर और राजस्व
-
भूमि कर, जल कर, व्यापार कर आदि प्रमुख स्रोत थे।
-
किसानों से 1/4 तक उपज का कर लिया जाता था।
5. गुप्तचर तंत्र
-
चंद्रगुप्त का गुप्तचर विभाग बहुत मजबूत था। चाणक्य की नीति में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
-
गुप्तचर दो प्रकार के होते थे – बाह्य और आंतरिक।
6. सैन्य संगठन
-
विशाल स्थायी सेना थी। इसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और हाथी शामिल थे।
-
यूनानी लेखक मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना में लगभग 6 लाख सैनिक थे।
7. अर्थव्यवस्था
-
कृषि, व्यापार, उद्योग, खनन आदि को सरकारी संरक्षण प्राप्त था।
-
‘अर्थशास्त्र’ ग्रंथ में पूरी आर्थिक संरचना का वर्णन है।
8. चाणक्य का योगदान
-
उन्होंने नीति, प्रशासन, कर व्यवस्था, न्याय और अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार किया।
-
चंद्रगुप्त के शासन की स्थिरता और सफलता में उनकी भूमिका अनमोल रही।
🕊️ भाग 4: चंद्रगुप्त का जैन धर्म की ओर रुझान और अंतिम जीवन
1. सन्यास की भावना
शासन के कई वर्षों बाद चंद्रगुप्त मौर्य के भीतर वैराग्य की भावना जागृत हुई। युद्ध, राजनीति और राज्य के उत्तरदायित्वों से निवृत्त होकर उन्होंने आध्यात्मिक शांति की ओर कदम बढ़ाया।
2. भद्रबाहु से संपर्क
इस काल में जैन धर्म के महान आचार्य भद्रबाहु भारत के प्रमुख तपस्वी थे। चंद्रगुप्त उनके शिष्य बने और जैन धर्म की दीक्षा ली।
3. श्रवणबेलगोला की यात्रा
भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की यात्रा की और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर तपस्या में लीन हो गए।
4. सल्लेखना व्रत
जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने सल्लेखना व्रत (अर्थात धीरे-धीरे उपवास करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना) का पालन किया। यह व्रत आत्मशुद्धि और मोक्ष की ओर अंतिम कदम माना जाता है।
5. मृत्यु
चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 297 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्यागे। यह स्थान आज भी जैन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। वहाँ उनकी स्मृति में विशाल चंद्रगुप्त बस्ती और भद्रबाहु गुफा स्थित है।
6. विरासत
-
उन्होंने भारत में पहले बड़े सम्राट के रूप में एक संगठित, शक्तिशाली और सुसंस्कृत साम्राज्य की नींव रखी।
-
उनकी नीति, शासन प्रणाली और कूटनीति आज भी राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए प्रेरणा है।
-
उनका जीवन संघर्ष, नेतृत्व और आत्मनियंत्रण का उदाहरण है।
यह जीवनी श्रृंखला अब पूर्ण हो चुकी है। कृपया अपनी राय और सुझाव साझा करें, और आगे की ऐतिहासिक जीवनी पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

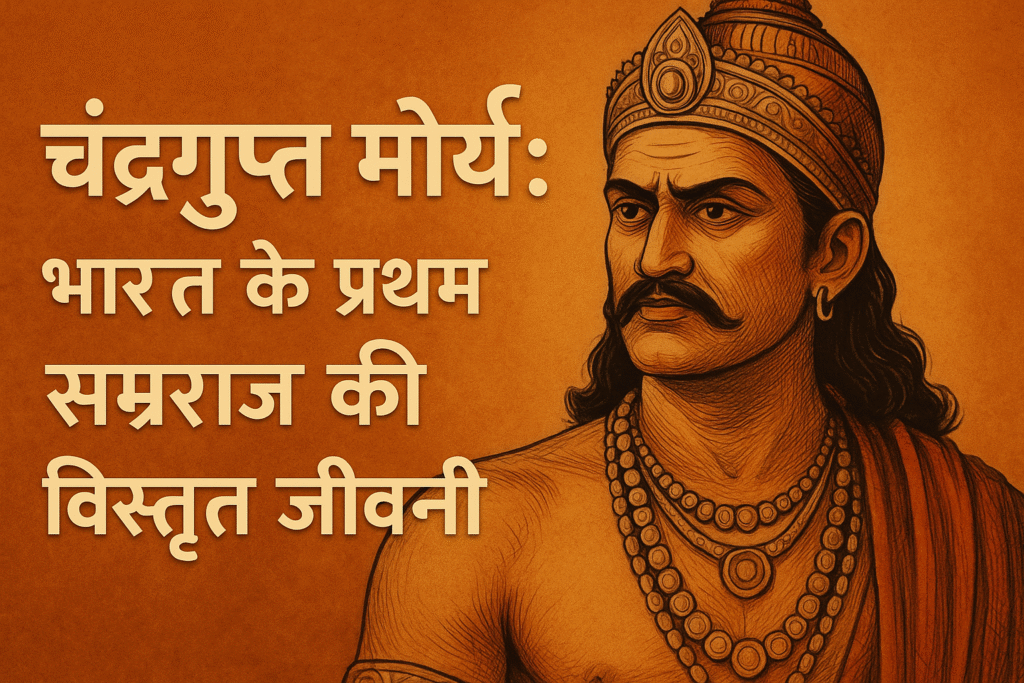

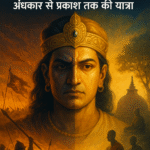
Good 👍